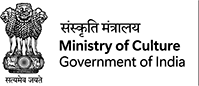वेदों में विधिव्यवस्था
विधि शब्दार्थ – विधिशब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार वि उपसर्गपूर्वक धा धातु में कि प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, जिसका अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। यथा- करना, अनुष्ठान, अभ्यास, कृत्य, कर्म, प्रणाली,रीति, पद्धति, साधन, ढंग, नियम, समादेश, न्याय, कानून, तरीका आदि। विधि का एक अर्थ ब्रह्मा भी होता है। वेदों में प्राप्त विश्वसृष्टि प्रक्रिया के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्मा सर्वप्रथम अपनी महिमा से जड़चेतनात्मक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकट करता है। तत्पश्चात् उसके सञ्चालन,संरक्षण एवं नियन्त्रण हेतु कुछ नियम बनाता है, जिसे विधि का विधान कहते हैं। वि उपसर्गपूर्वक धा धातु में ल्युट् प्रत्यय करने पर विधान शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ- क्रम से रखना,व्यवस्था करना, नियोजन, उपयोग, प्रयोग आदि होता है। उसी विधान के अनुसार संसार का समस्त कार्य सुचारुतया व्यवस्थित क्रम से चलता रहता है। वह विधि का निर्माता तथा विधानकर्त्ता है, अतः विधाता कहलाता है। लोक में कोई विधाता तो नहीं होता किन्तु तत्सदृश कार्य करने के कारण तद्वत् सम्मान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विधि शब्द के उपर्युक्त अर्थों को अपनाता है वह विधायक कहलाता है, तथा उपर्युक्त अर्थों के पालनार्थ जो समय-समय पर निर्देश प्रदान करे किं वा किसी प्रकार की अवहेलना, या उलझन होने पर उचितानुचित को स्पष्ट करे वह संस्था विधायिका कहलाती है। विधि को जाननेवाला विधिज्ञ, विधि का प्रमाण सहित सोदाहरण व्याख्या करनेवाला अधिवक्ता तथा अनुपालन का निर्देश देनेवाला, उचितानुचित का निर्णय करनेवाला- निर्णायक, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आदि शब्दों से व्यवहृत होता है।विधि का पर्याय न्याय एवं आचार- विधि का पर्याय न्याय शब्द सम्प्रति बहुप्रचलित है। इसलिए यह न्याय का कार्य जहाँ होता है, उसे न्यायालय, न्याय करनेवाले को न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आदि शब्दों से पुकारा जाता है। न्याय किसी न किसी नीति पर आधारित होता है। नीतियों का निर्धारण देश, काल, परिस्थिति एवं पात्र के अनुसार किया जाता है। नीति निर्धारण में कुलपरम्परागत आचार का प्रमुख स्थान है। इस विषय में भगवान् मनु का कथन है कि-तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः। वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते।। [१]अर्थात् जिस देश में जो आचार विचार परम्परानुसार ब्राह्मणादि वर्णों के लिए पहले से प्रचलित है,अर्थात् नवनिर्मित नहीं है, या कपोल कल्पित नहीं है, उस देश एवं वर्ण का वही कुलपरम्परागत आचार सदाचार शब्द से व्यवहृत होता है। आचार को परम धर्म कहा गया है, तथा आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते यह भी कहा गया है। अतः आचार को प्रथम धर्म भी कहा गया है। आचार से ही सबकुछ प्राप्त होता है। यथा- आचारः परमो धर्मः [२], आचारः प्रथमो धर्मः [३], आचारवान्सदा पूताः [४], आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः [५], आचाराल्लभते ह्यायुः [६], जनः किलाचारमुचं विगायति। [७] इत्यादि अनेक शास्त्रेक्त वचन हमारे लिए पाथेय स्वरूप हैं, जिनके अनुपालन से हम अपने मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। यह आचार शास्त्रीय एवं लौकिक भेद से दो प्रकार का कहा गया है, दोनों प्रकार के आचार का पालन ही धर्म है। अतः आचारशब्द धर्म शब्द से व्यवहृत है। जिसे हम धारण करते हैं, उसे ही धर्म कहते हैं। आचार को सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। यथा- सर्वधर्मवरिष्ठोडयमाचारः परमं तपः। तदेव ज्ञानमुद्दिष्टं तेन सर्वं प्रसाध्यते।। [८]वस्तुतः इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन्हें तीन कोटियों में रखा जा सकता है- सारग्राही,भारवाही एवं जिज्ञासु। इन तीनों में प्रथम अत्यल्प हैं तथा शेष दोनों कोटि के मनुष्य बहुत मिलते हैं। सारग्राही दो प्रकार के होते हैं- ऋषि एवं मुनि। मन्त्रसूक्तादिकों के द्रष्टा ऋषि तथा दर्शनादि शास्त्रप्रवक्ता मुनि कहलाते हैं। भारवाही भी दो प्रकार के होते हैं- प्रथम स्वयं को पण्डित माननेवाले वितण्डावादी तथा द्वितीय ज्ञानबलदुर्विदग्ध धूर्त एवं धृष्टचरित। इसी प्रकार जिज्ञासु भी दो प्रकार के होते हैं- मूर्ख एवं विनीत। इनमें से जो विनीत है उसके लिए ही समस्त शास्त्रें की प्रवृत्ति कही गई है। क्योंकि विद्या ने स्वयं ब्राह्मण के पास आकर यह निवेदन किया है कि-विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां सेवधिष्टेह हमस्मि। असूयकायानृजवेह यताय न मा ब्रूयाः वीर्यवती तथा स्याम्।। [९]उक्त कथन का यह अभिप्राय है कि एकबार विद्या ब्राह्मण के पास आकर उनसे निवेदन कर कहा कि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी सेवा के अन्तर्गत हूँ। जो ईर्ष्यालु या निन्दक हो, कुटिल या अयोग्य हो तथा अनियन्त्रित हो उसे मेरा उपदेश कभी मत करना। इस उद्धरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि समस्त शास्त्रें का उपदेश मात्र विनीत मनुष्यों के लिये ही किया गया है।न्याय का धर्मस्वरूप-विनीतों का आचारवान् होना भी आवश्यक है। आचारहीन मनुष्य धर्मरूप न्यायव्यवस्था को कथमपि सुरक्षित नहीं रख सकता है। धर्म की रक्षा से ही सबकी रक्षा सम्भव है। कहा भी गया है- धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। [१०] अर्थात् धर्म के नष्ट होने पर सबकुछ नष्ट हो जाता है तथा धर्म की रक्षा से सबकी रक्षा होती है।सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल अर्थ या धन है। अर्थ का मूल राज्य है। राज्य का मूल इन्द्रियविजय या संयम है। इन्द्रियविजय का मूल विनय या शील है। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा है- सुखस्य मूलं धर्मः। धर्मस्य मूलमर्थः। अर्थस्य मूलं राज्यम्। राज्यमूलमिन्द्रियविजयः। इन्द्रियविजयस्य मूलं विनयः। [११]किसी भी राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए या सुचारुतया सञ्चालन के लिए आचार एवं नीति आवश्यक होती है। यद्यपि आचार एवं नीति एक होते हुए भी दोनों में सूक्ष्म भेद है। आचारशिक्षा का सम्बन्ध वैयक्तिक जीवन से है। इसमें आत्मोन्नति पर विशेष बल दिया गया है। नीतिशिक्षा में सामाजिक, राष्ट्रीय, विश्वजनीन विषय भी समाहित हैं। इस विषय पर वेदों में बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध है तथापि उनमें से कुछ आवश्यक मन्त्रें को उद्धृत कर रहा हूँ।नीति शिक्षा- नीतिशिक्षा जीवन के व्यापक स्वरूप को प्रकट करती है। मनुष्य अपने, पराए, सजातीय, विजातीय, शत्रु, मित्र, परिचित, अपरिचित आदि से किस प्रकार व्यवहार करे, इसकी शिक्षा नीतिशिक्षा देती है। सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति के क्या साधन हैं? जीवन की क्या उपयोगिता है? बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं के के प्रति क्या व्यवहार रखा जाए? अनर्थकारी प्रवृत्तियों को कैसे रोका जाए? व्यक्ति का विश्वशान्ति, विश्वबन्धुत्व और विश्वसंस्कृति में क्या उपयोग हो सकता है? इत्यादि विभिन्न विषयों पर चिन्तन नीतिशिक्षा के अन्तर्गत आता है। ये समस्त विषय संविधान में प्रतिपादित होते हैं। इसलिए विविध नीतियों के संकलन को संविधान कहा जाता है। सं सम्यक् विधीयन्ते सर्वाण्यप्युचितानि कर्माणि येन शास्त्रेण तत् संविधानम् इस व्युत्पत्ति से संविधान आचार एवं नीति का सैद्धान्तिक शास्त्र सिद्ध होता है।नीतियों को भी तीन कोटि में विभाजित किया जा सकता है- धर्मनीति, राजनीति एवं विज्ञाननीति। मानव के कर्त्तव्य एवं अधिकारों की चर्चा जहाँ हो उसे धर्मनीति, शत्रुओं का दमन एवं स्वराष्ट्र की भौतिक उन्नति की बात जहाँ हो उसे राजनीति तथा आध्यात्मिक विकास की चर्चा जहाँ हो उसे विज्ञाननीति कहा जा सकता है।महाकवि माघ ने शिशुपालवध महाकाव्य में नीतिशास्त्र का लक्षण करते हुए कहा है- आत्मोदयः परग्लानिर्द्वयं नीतिरितीयती। [१२] अर्थात् अपनी उन्नति और शत्रुओं का विनाश ये दो बातें नीति में मुख्य हैं। वस्तुतः नीति का यह लक्षण राजनीति से सीधा सम्बन्ध रखता है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई व्यक्ति समान लम्बाई चौड़ाई और मोटाई के दो डंडे लाकर सामने रख दे और यह कहे कि इसमें से एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कर दीजिए तो इस कार्य को करने के लिए हम दो विधियों का आश्रय ले सकते हैं।1- दोनों डंडों में से किसी एक डंडा में कहीं अन्यत्र से कोई छोटा टुकड़ा लाकर जोड़ देने से एक छोटा और एक बड़ा हो जाएगा।2- दोनों डंडों में से किसी एक डंडा का कुछ भाग तोड़कर हटा देने पर एक छोटा और दूसरा बड़ा रह जाएगा।इस प्रकार महाकवि माघ के कथनानुसार आत्मोदय एवं परग्लानि नीति की ये दो विधियाँ अत्यन्त व्यावहारिक सिद्ध हो रही हैं। इन दोनों विधियों में प्रथम तो धर्मनीति के पक्ष को प्रबल माना है जिसमें अपनी अभ्युन्नति तो है परन्तु किसी की हानि नहीं। दूसरी विधि उसके ठीक विपरीत है जो राजनीति के पक्ष को प्रबल मानकर प्रयुक्त है, जिसमें दूसरे को हानि पहुँचाकर अपनी अभ्युन्नति प्रदर्शित की गई है। इन दोनों विधियों में कौन श्रेष्ठ है? यदि यह पूछा जाय तो प्रथमविधि को सभी पसन्द करेंगे। विज्ञाननीति में किसी को छोटा या बड़ा समझने व करने की बात ही नहीं है, वह तो भौतिकता से परे आत्मानन्द की प्राप्ति में सहायक है।वैदिक विधि व्यवस्था- वेद में इन समस्त विधियों का विस्तृत विवेचन कर्त्तव्य के रूप में किया गया है। लघुनिबन्ध में उन सबका समावेश सम्भव नहीं, अतः कुछ मन्त्रें को उद्धृत किया जा रहा है। यथा-सबसे पहले तो अशुभलक्षणों, दुर्गुणों को दूर करने तथा शुभलक्षणों, सद्गुणों को प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। जैसे- विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आसुव।। [१३] तत्पश्चात् पुरुषार्थ से सांसारिक सुखों व सफलताओं को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है-कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः। गोजिद् भूयासमश्वजिद् धनञ्जयो हिरण्यजित्।। [१४]अर्थात् मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है तथा वाएँ हाथ में विजय है। मैं गाय, अश्व, धन एवं सुवर्णादि द्रव्यों को जीतने वाला होउँ, यह कामना की गई है। इसके साथ-साथ कुछ अन्य उपाय एवं संसाधनों की बात गई है। यथा-सम्राडस्यसुराणां ककुन्मनुष्याणाम्। देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव।। [१५]प्रस्तुत मन्त्र में मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ होकर जीवित रहे इसके तीन उपाय बताये गये हैं- (1)असुरों का दमन करना, (2) मनुष्यों में अग्रगण्य होना तथा (3) देवों का आधा भाग भोगना। मन्त्र का उपदेश है कि हे वीर मनुष्यो! तुम असुरों के (सम्राट्) स्वामी हो, तुम मनुष्यों में मूर्धन्य हो, तुम देवों के आधे भाग के अधिकारी हो, तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ होओ।मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए उच्चकोटि का ज्ञान, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, और उत्कृष्ट मनोबल होना चाहिए। ज्ञानी, विद्वान्, सदाचारी, परोपकारी और उदारमना व्यक्ति ही मनुष्यों में अपना स्थान सर्वोच्च बना सकता है।आरादरातिं निऋतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान्। रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवाप हन्मसि।। [१६]इस मन्त्र में कतिपय दूषित तत्त्वों को नष्ट करने का विधान है। इनमें कुछ व्यक्तिगत जीवन से सम्बद्ध हैं और कुछ समाज से। शत्रु, दुर्गति और रोग व्यक्ति से सम्बद्ध हैं। क्रव्याद्, पिशाच और राक्षस समाज से संबद्ध हैं। इन सभी अहितकर तत्त्वों को अन्धकार की तरह बहुत दूर से ही नष्ट करते हैं।मन्त्र का कथन है कि सभी दोषों को इसी प्रकार नष्ट करें, जैसे प्रकाश अन्धकार को नष्ट करता है। इनमें से अराति या शत्रु को अपने उत्साह से, दुर्गति या कष्टमय जीवन को पुरुषार्थ से, रोगों को नियमों के पालन, नियमित आहार तथा व्यायामादि से, हिंसक जन्तुओं को आयुधों से,मांसाहारियों को सामाजिक बहिष्कार या उपदेश से, दुष्टों, पापियों और अत्याचारियों को कठोर दण्ड से नष्ट किया जा सकता है। समाज एवं राष्ट्र की समृद्धि के लिए ऐसे दूषित तत्त्वों को नष्ट करना आवश्यक है।दुष्ट के दो रूप कहे गये हैं- प्रकट एवं गुप्त। प्रकट दुष्ट की अपेक्षा गुप्त दुष्ट अधिक घातक तथा कष्टकारी होते हैं। इस प्रकार के दुष्टों के विनाशार्थ मरुत् देव से प्रार्थना की गई है-यो नो मर्तो मरुतो दुर्हणायुः तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति। द्रुहः पाशान् प्रति मुञ्चतां सः तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम्।। [१७]अर्थात् हे मरुत् देव! छुपकर हानि पहुँचाने वाले दुर्भावनाग्रस्त प्रच्छन्न दुष्टों को कठिन से कठिन (अत्यन्त सन्तापकारी) दण्ड देकर मारो।वेद में शत्रु का समूल नाश करने के लिए शस्त्रस्त्रें से प्रार्थना की गई है। यथा-अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसं सिते। गच्छामित्रन् प्र पद्यस्व मामीषां कञ्चनोच्छिषः।। [१८]तीन प्रकार की शक्ति कही गई है- मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति और प्रभुशक्ति। मन्त्रशक्ति वस्तु में सजीवता प्रदान करने के कारण तीनों शक्तियों में प्रमुख है। मन्त्रशक्ति से तीक्ष्ण किये हुए अस्त्र को शत्रु पर प्रक्षिप्त करते हुए कहा गया है कि- हे क्षेप्य अस्त्र! यहाँ से फेंका हुआ तू दूर जाकर शत्रुओं के पास पहुँच। इन शत्रुओं में से किसी को मत छोड़ना।वेद में यह स्पष्ट कहा गया है कि शत्रु को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि छूटा हुआ शत्रु अवसर पाकर अवश्य हानि पहुँचायेगा। अतः जिस प्रकार भेड़िया भेड़ को रगड़ कर मार डालता है उसी प्रकार शत्रु को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहिए। यथा-अति धावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा हत। अविं वृक इव मथ्नीत स वो जीवन् मा मोचि, प्राणमस्यापि नह्यत।। [१९]तात्पर्य यह है कि शत्रु यदि वश में आ गया हो तो उसे छोड़ना उचित नहीं है। इस विषय में चाणक्य का कथन है कि- ऋणशत्रुव्याधिष्वशेषः कर्तव्यः इति। [२०] अर्थात् ऋण, शत्रु एवं व्याधि को जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। विदुरनीति में भी यही कहा गया है-न शत्रुर्वशमापन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गतः। न्यग्भूत्वा पर्युपासीत वध्यं हन्याद् बले सति। अहताद्धि भयं तस्माद् जायते न चिरादिव।। [२१]वेद में अकर्मण्य को समाज का शत्रु कहा गया है। वेद का उपदेश है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्। [२२] किन्तु जो अकर्मण्य है, चोर है, अज्ञानी है, कुकर्मी है तथा मानवोचित आचार-विचार से रहित है, वह अपने कर्मों के कारण समाज को क्षति पहुँचाता है। ऐसे समाजघातकों को देश का शत्रु कहा गया है। उसके रहते परिवार, समाज और राष्ट्र का अभ्युत्थान नहीं हो सकता। अतः ऐसे शत्रुओं के विनाश की प्राथमिकता दी गई है। यथा-अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः। त्वं तस्यामित्रहन् वधर्दासस्य दम्भय।। [२३]अर्थात् काम न करनेवाला अकर्मण्य चोर के तुल्य है। वह हमें कुछ नहीं मानता है। वह कुकर्मों में लगा रहता है और मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। हे शत्रुओं के नाशक इन्द्र! तुम उस दास को नष्ट करो।एक मन्त्र में पाप के पाँच कारणों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ कारण नियति के अन्तर्गत हैं जिनपर मावनीय प्रयासों का कोई असर नहीं हो पाता, किन्तु जिन कारणों पर उसका प्रभाव हो सकता है, उन कारणों को न्यायविद् जानकर उसके रोकथाम का उपाय बताते हुए उसे तत्काल प्रभाव से रोकने का आधिकारिक आदेश जारी करें तो पाप एवं पापियों की अभिवृद्धि को रोका जा सकता है। यथा-न स स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः। [२४]यहाँ ध्रुति शब्द नियति (प्रारब्ध अर्थात् प्राग्जन्मकृत कर्म) का वाचक है, सुरापान, क्रोध, जुआ और अज्ञान ये पाँच पाप के कारण कहे गये हैं।उपर्युक्त सब प्रकार के पापियों को नियन्त्रित करने के लिए परमात्मा ने दण्ड का विधान किया है। कठिन शत्रु का प्रतीकार कठिन दण्ड से करने का विधान वेद में किया गया है। नैयायिकों को उसका आश्रय लेना चाहिए तथा शत्रुओं को किसी प्रकार स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए। अपितु दुर्जनों से यथायोग्य व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। यथा-अरसास इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके। घनेन हन्मि वृश्चिकं अहिं दण्डेनागतम्।। [२५]तात्पर्य यह है कि दुर्जन किसी भी रूप में हों, वे समाज के लिए हितकर नहीं हैं। दुर्जन समाज और राष्ट्र के उत्पीडन में लगे रहते हैं। वे अन्याय और अत्याचार से परशोषण करते हैं। उन्हे सामाजिक या राष्ट्रीय हित की चिन्ता नहीं होती है, अतः लीतिविदों ने उन्हें यथायोग्य दण्ड देने का विधान किया है। इसी दृष्टि से उक्त मन्त्र में कहा गया है कि यहाँ जो पास में या दूरी पर साँप हैं, वे सारहीन हो जाएं। मैं बिच्छू को हथौड़े से मारता हूँ और पास आये साँप को डंडे से मारता हूँ।एक मन्त्र में समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पापी को कठिन से कठिन दण्ड देने का विधान किया गया है। यथा-इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्यस्तु चरुरग्निवाँ इव। ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षुषे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने।। [२६]अर्थात् हे इन्द्र और सोम देवो! तुम दोनों पापकर्म में लिप्त पापी को अच्छी तरह तिरस्कृत करो। आग पर रखी हुई हांडी की तरह दुःख देनेवाला व्यक्ति तपाया जाए। नास्तिक, मांसाहारी, क्रूर दृष्टि और सर्वभक्षक व्यक्ति पर तुम दोनों निरन्तर द्वेष का भाव रखो। यहाँ पाँच प्रकार के पापियों का उल्लेख है- अघशंस- दूसरे का बुरा सोचनेवाल, ब्रह्मद्विष- नास्तिक एवं एवं ज्ञान का द्वेषी, क्रव्याद- मांसाहारी, घोरचक्षुष्- बुरी दृष्टि से देखनेवाला तथा किमीदिन्- सर्वभक्षी या भक्ष्य-अभक्ष्य का विचार न करने वाले। ये सब कुत्सित कर्म में लिप्त रहने के कारण आचारहीन होते हैं। अतः समाज एवं राष्ट्र के लिए हानिकारक एवं दण्डनीय हैं।छान्दोग्योपनिषद् के- न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः।नानाहिताग्निर्नाविद्वान्त स्वैरी स्वैरिणी कुतः।।[२७]इस कथन से स्पष्ट होता है कि वैदिककाल में सुशासन होने के कारण किसी भी राजा के राज्य में स्तेन आदि पापी नहीं रहते थे। किन्तु सर्वथा नहीं थे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि शुक्लयजुर्वेद के सोलहवें अध्याय में सात प्रकार के चोरों की चर्चा की गई है। चथा-1. स्तेन- घर में सेंध मारकर गुप्तरूप से चोरी करनेवाले।2. स्तायु- रात दिन अज्ञान रूप से चोरी करनेवाले। ऋग्वेद में वस्त्र चुरानेवाले को तायु [२८] कहा गया है।3. तस्कर- प्रकट रूप से चोरी करनेवाले।4. मुष्णन्तः- खेत में धान चुरानेवाले।5. निचेरव- चुराने की इच्छा से निरन्तर विचरण करनेवाले।6. परिचर- बाजार तथा फूलवारी आदि में चुराने की इच्छा से घूमनेवाले।7. कुलुञ्च- खेत, घर आदि को लूट लेनेवाले।इन समस्त पापियों को कठिन दण्ड देने का विधान वेदों में प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ गाय, अश्व एवं मानवों की हत्या करने वालों के शरीर को शीशे से बेधने का दण्डविधान प्राप्त होता है। यथा-यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम्। तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो सो अवीरहा।। [२९]इस प्रकार वेद के अनेक मन्त्रें में समाज एवं राष्ट्रहित के लिए उचित न्यायव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इन्हीं मन्त्रवाक्यों के आधार पर विविध नीतिशास्त्रें का प्रवर्तन प्राचीन आचार्यों द्वारा किया गया है। वे सब शास्त्र वेदमूलक होने के कारण सर्वत्र मान्य, पूज्य एवं श्रद्धा के योग्य हैं। धर्म से सम्बन्धित समस्त विषयों का विस्तृत विवेचन धर्मशास्त्रदि ग्रन्थों में किया गया है। वहाँ तो देश, काल, परिस्थिति एवं पात्र के अनुसार समुचित दण्डविधान किया गया है। किस प्रकार के अपराध का क्या, कितना और कैसा दण्ड हो? न्यायकर्ता कैसा हो? न्याय का स्वरूप क्या हो? इन सब प्रकार के विषयों पर तत्तत् शास्त्रें में अत्यन्त सूक्ष्मतया विचार किया गया है। उन सभी ग्रन्थों का आश्रय लेकर हमें विधि को व्यवस्थित करनी चाहिए। चूँकि विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेदः यह वेद का एक लक्षण है। विधिशब्द ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वहाँ किस कर्म का क्या प्रायश्चित्त हो इसपर विचार किया गया है। तर्कशब्द मीमांसा एवं न्यायशास्त्र के लिए प्रयुक्त है। इन सबों को मिलाकर वेद है। अतः वेद एवं वैदिकसाहित्य का आलोडन, अन्वेषण एवं परिशीलन होता रहना चाहिए। सम्प्रति उक्त शास्त्रें का अध्ययन-अध्यापन समाज एवं राष्ट्र के हित में परमावश्यक है। मनुष्यों का नैतिक पतन होना स्वाभाविक है। शतपथब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि नैव देवा (प्रजापतेराज्ञाम्) अतिक्रामन्ति। न पितरो न पशवो मनुष्या एवैके [३०] तिक्रामन्ति। अर्थात् सृष्टिकर्ता विधाता की आज्ञा (नियम) की अवहेलना न देवता करते हैं, न पितर और न ही पशु करते हैं। केवल मनुष्य ही नियमों को तोड़ता है। अतः ये समस्त संविधान केवल मनुष्यों (मानवों) के लिए ही है। मानव मनु की सन्तान है, इसलिए मनु द्वारा निर्मित धर्मशास्त्र का स्वाध्याय परमावश्यकतया होना चाहिए, जिससे मानव के आचार, विचार एवं व्यवहार में शुद्धता बनी रहे। आचारहीन होने के कारण ही ये समस्याएँ होती रही हैं, इस ओर हमें अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।निष्कर्ष-विधिव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करना है। एतदर्थ सन्मार्ग के लिए सबको प्रेरित करना, अधर्म के कारणों का ज्ञान करना तथा उसको रोकना, अपराधी प्रवृत्ति का समूल विनाश हो तदर्थ उचित दण्ड की व्यवस्था करना, पापाचारियों को कठिन सन्ताप द्वारा उसे अपने कुकर्म का ज्ञान कराकर पश्चात्ताप कराना। सामाजिक उन्नति में बाधक तत्त्वों को दण्डित करना, सभ्यता-संस्कृति, आचार-विचार एवं परम्पराओं तथा मर्यादाओं की रक्षा हेतु वेदादि शास्त्रें में प्रदर्शित नियम, उपनियम एवं विनियमों के पालनार्थ सदा जनजागृति का कार्य करना परमावश्यक है।वेद का उपदेश है कि विश्व के समस्त मानव को सदा जागरूक रहना चाहिए। एतदर्थ गार्हपत्याग्नि को लक्ष्य बनाकर निम्न मन्त्र प्रस्तुत है-त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः।सपत्नहाग्ने अभिमातिजिद् भव स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन्।। [३१]अर्थात् हे गार्हपत्य अग्नि! ये ब्राह्मण तुम्हें स्वीकार करते हैं। हे अग्नि! तुम हमारे निवासस्थानों में सुखद होओ। हे अग्नि! तुम शत्रुनाशक और कपटी लोगों के नाशक होओ। अपने घर में प्रमादरहित रहते हुए सदा जागरूक रहो।इस मन्त्र में गार्हपत्याग्नि की जागरूकता के प्रदर्शन द्वारा गृहस्थों की जागरूकता पर बल दिया गया है। जिस प्रकार अग्नि अपने स्थान में सदा जागरूक रहती है, उसी प्रकार गृहस्थों को भी अपने घर में सदा जागरूक और सावधान रहना चाहिए। प्रमाद या असावधानी ही विपत्ति के कारण बन जाते हैं।अग्निष्टोमयाग प्रसङ्ग में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि तुम जागो और हम सोयें। यथा- अग्ने त्वां सु जागृहि वयां सु मन्दिषीमहि। रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधे नः पुनस्कृधि।। [३२] तात्पर्य यह है कि अग्नि हमारा रक्षक तथा राक्षसों का अपहन्ता है। राक्षस शब्द यहाँ पारिभाषिक है जिसका अर्थ समाज के विघातक शत्रु गुप्त एवं प्रकट चोरों से है। इस प्रकार अग्नि यहाँ न्यायमूर्त्ति के रूप में स्तुत्य हुआ है। न्यायमूर्त्ति चोरों, अपराधियों एवं कुकर्मियों के लिए अग्नि के समान सन्तापक होता है। यज्ञसंस्था यहाँ विधायिका किंवा न्यायालय के रूप में प्रस्तुत है, तथा यजमान सत्यानुष्ठानकर्त्ता है, जिसकी रक्षा विधिव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है।यह सबकुछ समक्ष होते हुए भी मानवमात्र को सदा जागरूक रहने की प्रेरणा दी गई है। क्योंकि जागरूक को ही सफलता मिलती है। यथा-यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति।यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः।। [३३]अर्थात् जो जागता है उसको ही ऋग्वेद के मन्त्र चाहते हैं। जो जागता है उसके पास ही सामवेद की ऋचाएँ आती हैं। जो जागता है उससे सोम कहता है कि मैं तुम्हारी मित्रता में प्रसन्नचित्त रहता हूँ। वेदों में मित्रता की अत्यन्त प्रशंसा की गई है। मैत्रीभाव अभयता को प्रदान करता है। अतः संसार का समस्त मानव मित्रभाव से संगठित होकर रहे, जीवन यापन करे और सब अपने-अपने कार्य में तल्लीन रहे, वेद में स्थान-स्थान पर यह उद्घोष किया गया है।जो जागता है उसके पास ऋग्वेद और सामवेद के मन्त्र आते हैं इस कथन का तात्पर्य यह है कि वेदों में समस्त गूढतम विद्याएँ व्याप्त हैं। उन रहस्यों का ज्ञान उसी को हो पाता है जो सूक्ष्म बुद्धिवाला है तथा सतत उद्यमनशील, अध्ययनशील व जागरूक रहता है। सामान्य बुद्धि वाले उन रहस्यों से विञ्चत रह जाते हैं। अतः जो जागते हैं, सावधान हैं, प्रबुद्ध हैं, वे ही आत्मतत्त्व को जान पाते हैं। साधना का मार्ग इतना सूक्ष्म और गहन है कि जो असावधानी करेगा, वह अपने लक्ष्य से च्युत होगा। सावधानी से एवं सतत जागरूकता से इस मार्ग पर चलना होता है।जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। जयन्तु वेदाः।[१] मनुस्मृति-2/18[२] मनुस्मृति-1/108, दे-भा– 11/1/11[३] दे-भा– 11/1/19[४] दे-भा– 11/24/98[५] दे-भा– 11/2/1[६] मनुस्मृति-4/1/56, दे-भा– 11/1/10[७] नैषध-6/23[८] दे-भा–11/1/14[९] निरुक्त-2/1/4[१०] महाभारत, वनपर्व-313/128[११] चा- सूत्र-1-5[१२] शिशुपालवध-2/30[१३] ऋग्वेद – 5/82/5 , यजुर्वेद-30/3 , तै-ब्रा– 2/4/6/3[१४] अथर्ववेद-7/50/8[१५] अथर्ववेद-6/86/3[१६] अथर्ववेद- 8/2/12[१७] अथर्ववेद-7/77/2[१८] ऋग्वेद – 6/75/16, यजुर्वेद-17/45, अथर्ववेद-3/19/8[१९] अथर्ववेद-5/8/4[२०] चा-सू– 435[२१] विदुरनीति-6/29[२२] शु-य-सं– 40/2[२३] ऋग्वेद – 10/22/8[२४] ऋग्वेद – 7/86/6[२५] अथर्ववेद-10/4/9[२६] ऋग्वेद – 7/104/2, अथर्ववेद-8/4/2, निरुक्त-6/11[२७] छां. उप- 5/11[२८] ऋग्वेद- उतस्मैनं वस्त्रमथिं न नायुमनुक्रोशन्ति क्षितयो भरेषु 4/35/5[२९] अथर्ववेद- 1/16/4[३०] श-प-ब्रा-2/4/2/6[३१] यजुर्वेद-27/3, अथर्ववेद-2/6/3[३२] शु-य-सं– 4/14[३३] ऋग्वेद-5/44/14, सामवेद-1826